पेड़ मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं। ये हवा को शुद्ध कर और फल फूल प्रदान कर मानव जाति को लाभ पहुंचाते हैं। ऐसा ही एक पेड़ है बांज (ओक) का। इसे उत्तराखंड का हरा सोना कहा जाता है। हालांकि, यह देश के दूसरे इलाकों में कम पाया जाता है।
डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला
बांज पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को व्यवस्थित रखने में अहम भूमिका निभाता है। पर्यावरण को शुद्ध रखने में इसकी अहम भूमकि है। पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही इस पेड़ में औषधीय गुण भी होता है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसकी जड़ें इतनी गहरी और फैली हैं कि यह मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। मृदा संरक्षण में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जल संरक्षण में भी बहुत कारगर है। इस पेड़ के आसपास के इलाकों में जलस्तर बढ़ता है और सूखे की समस्या से राहत मिलती है। इसके कई औषधीय गुण अनोखे हैं। औषधि के रूप में यह रामबाण है। इस पेड़ की छाल को औषधि के रूप में इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर की समस्या से राहत मिलती है। बांज के पेड़ की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से ब्लड प्रेशर की समस्या से राहत मिलती है। बांज के छाल का काढ़ा पाचन तंत्र को मजबूत करता है और अपच की समस्या को दूर करता है। इसके साथ ही इसके पत्तों का काढ़ा डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं।
सामाजिक सरोकारों में भी यह पेड़ अहम भूमिका निभाता है। बांज की खेती करके आप लाखों रुपये कमा सकते हैं। बांज की खेती और इसके लकड़ी के व्यापार से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। कई संस्कृतियों में बांज के पेड़ों को पवित्र माना जाता है और धार्मिक अनुष्ठानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बांज की लकड़ी से कागज बनाया जाता है। बांज के पत्तों पर पाए जाने वाले रेशम के कीड़ों से रेशम भी बनाया जाता है। पर्यावरण, जल व मृदा संरक्षण और सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए हमें बांज के पेड़ की खेती अवश्य करनी चाहिए। हमें इसके पेड़ों की रक्षा और संरक्षण करना चाहिए, ताकि हम इससे लाभ प्राप्त कर सकें।
प्राकृतिक वनस्पति, पेड़-पौधों, औषधीय पौधों की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का एक सम्पन्न राज्य है और यहां प्राकृतिक हरियाली देखते ही बनती है। यहां की वनस्पति अक्षत वनस्पति है। अक्षत यानी कि एक प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति। वास्तव में प्राकृतिक वनस्पति प्रकृति की देन होती है जो कि अपने आप पैदा होती है और जिस पर लंबे समय तक मानव का प्रभाव नहीं पड़ता है। फसलें, फल और बागान इसके अंतर्गत नहीं आते, हालांकि ये भी वनस्पति ही हैं। उत्तराखंड की जलवायु व मिट्टी अपने आप में अनोखी है और इसमें पेड़-पौधे और विभिन्न वनस्पतियां प्राकृतिक रूप से अपने आप विकास करतीं हैं। ओलियंडर, पॉइन्सेटिया और अमरूद यहां मुख्य पेड़ हैं।
यह कहना ग़लत नहीं होगा कि ये पेड़ राज्य की सीमाओं के भीतर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, प्रतीकात्मक और पारिस्थितिक मूल्य रखते हैं। वैसे तो यह पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं लेकिन कुछ प्रमुख प्रजातियों में क्रमशः बांज, बुरांस (उत्तराखंड का राज्य वृक्ष), कांस, देवदार, कुळें, चीड़, पय्यां, अयांर, माळू, ग्वीर्याळ, रंसुळा, कैल, रिंगाळ, सेमल, तोण, डेंकण, भ्योल या भीमल, खड़ीक, गैंठी, पीपळ, खर्सु, मोरु, कण्डाळ, मळसु, भंगेलु शामिल हैं। वैसे उत्तराखंड में देवदार, स्प्रूस और फर जैसे शंकुधारी वृक्षों का प्रभुत्व है। साल, सागौन और ओक जैसे चौड़े पत्तों वाले पेड़ भी यहां प्रमुख हैं।
सच तो यह है कि उत्तराखंड भारत के कुछ सबसे विविध और सुंदर जंगलों का घर है। यहां उप-उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर अल्पाइन वनों तक, विभिन्न प्रकार के वनों की एक श्रृंखला है। ये जंगल पौधों और जानवरों की कई प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं, साथ ही स्थानीय समुदायों के लिए संसाधन भी प्रदान करते हैं। वैसे उत्तराखंड उपोष्णकटिबंधीय वन, उपोष्णकटिबंधीय शुष्क वन, उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, कोणीय वन, पर्वतीय समशीतोष्ण वन, अल्पाइन वन, अल्पाइन झाड़ियां तथा घास के मैदान और टुंडा वन समेत कुल आठ प्रकार के वनों का घर है। ओलियंडर, पाइंसेंटिया, लालफ्रैन्जी पैनी, अमरूद, गोल्डन शावर ट्री, काला टिड्डा, रेशमी ओक, पवित्र अंजीर, आड़ू, नीम, मीठी चेरी, नीला जकारांडा, देवदार, पीला ओलियंडर, पपीता, कपूर का पेड़, आर्किड वृक्ष, नोरफोक द्वीप पाइन, अनार और आम यहां के प्रमुख पेड़ हैं।

इन सभी के बीच जानकारी देना चाहूंगा कि बांज नामक पेड़ को उत्तराखंड का सोना कहां जाता है। बांज नामक पेड़ का बहुत महत्व है। बांज या बलूत या शाहबलूत एक तरह का वृक्ष है जिसे अंग्रेज़ी में ‘ओक’ कहा जाता है। बांज फागेसिई कुल के क्वेर्कस गण का एक पेड़ है। इसकी लगभग 400 के आसपास किस्में ज्ञात हैं, जिनमें कुछ की लकड़ियां बड़ी मजबूत और रेशे सघन होते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसके पेड़ भारत के अलावा अनेक देशों, पूरब में मलेशिया और चीन से लेकर हिमालय और काकेशस क्षेत्र होते हुए, सिसिली से लेकर उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र तक में पाये जाते हैं। इसकी पहचान इसके पत्तों और फलों से होती है। इसके पत्ते खांचेदार होते हैं और फल सामान्यतः गोलाकार और ऊपर की ओर नुकीला होता है। नीचे प्याले के ऐसे अनेक सहचक्र शल्क लगे रहते हैं।
कुछ बांज फल मीठे होते हैं और कुछ कड़ुए। कुछ बांज फल खाए जाते हैं और कुछ से टैनिन प्राप्त होता है, जो कि चमड़ा पकाने में काम आता है। बांज के फल सूअरों को भी खिलाए जाते हैं। खाने के लिए फलों को उबालकर, सुखाकर और आटा बनाकर केक बनाते हैं। उबालने से टैनिन निकल जाता है। यह सबसे अधिक उपयोग में आने वाला पर्यावरण का अहम् रक्षक पेड़ है। इस पेड़ की उत्तराखंड में कुल पांच प्रजातियां पाई जाती हैं। सच तो यह है कि बांज का पेड़ सदाबहार पेड़ है जो वर्षभर हरा भरा रहता है। वर्षभर हरा भरा रहने के कारण यह चारे की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बांज के पेड़ की पहाड़ी क्षेत्र की भूमि में नमी कायम रखने, जल संसाधनों की पूर्ति करने में अहम् भूमिका है।
जहां पर बांज के पेड़ पाये जाते हैं वहां आसपास पानी की प्रचुर उपलब्धता (पानी का चश्मे आदि) रहती है। नालों, धाराओं का सतत प्रवाह बनाए रखने में बांज के वृक्ष काफी सहायक सिद्ध होते हैं। यह पेड़ मिट्टी के कटाव को रोके रखता है। खनिजों से गुणवत्ता बढ़ाने में भी बांज के पेड़ का उल्लेखनीय योगदान रहता है। यह पेड़ पर्यावरण व विभिन्न प्राकृतिक क्रियाओं में संतुलन बनाए रखने में भी मददगार साबित होता है। वास्तव में बांज का पेड़ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की दैनिक व आर्थिक क्रियाओं से भी जुड़ा हुआ है। यह धीमी गति से बढ़ता है और इसका घनत्व अधिक होने के साथ साथ ही यह कठोर होता है और ठंड प्रधान क्षेत्रों में पैदा होता है। इसकी जड़ें गहरी, लंबी होने व भूमि में इनका अधिक फैलाव होने के कारण ये मिट्टी का कटाव नहीं होने देती और भूस्खलन होने से बचाव होता है।
बांज के पेड़ मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ ही पर्यावरण का भी स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करते हैं। हालांकि बांज भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम करते हैं लेकिन इसकी पत्तियां सड़ गलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती हैं। यह अन्य कई प्रकार की विशिष्ट वनस्पति प्रजातियों को फलने-फूलने के लिए उचित वातावरण भी प्रदान करता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण बरसात के दिनों में देखा जा सकता है जब बांज के तने एवं शाखाओं को अनेक प्रकार की वनस्पति की प्रजातियां ढक लेती हैं जैसे औरकिड, मौस, फर्न, लाइकन इत्यादि इत्यादि। जानकारी देना चाहूंगा कि उत्तराखंड में बांज के वनों का विस्तार विभिन्न ऊंचाइयों पर मुख्य रूप से नम तथा उत्तरी ढलानों में पाया जाता है। सामान्यतः ये वन समुद्र तल से 1200 मीटर (4000 फीट) की ऊंचाई से लेकर 2500 मीटर (8300 फीट) के मध्य पाये जाते हैं। इस वृक्ष की विभिन्न प्रजातियों में तिलांज बांज एवं खरसू बांज अत्यधिक ऊंचाई में पाये जाते हैं जबकि रियांज बांज मध्यवर्ती ऊंचाइयों में उगता है। फलियांट प्रजाति, जो बांज की भांति ही निचले एवं बसासत वाले क्षेत्रों की विशेषता है, बांज के समान विस्तृत रूप से नहीं पाई जाती। स्वाभाविक रूप से सभी प्रजातियों में बांज ही सबसे अधिक जानी भी जाती है और पाई भी जाती है।
वास्तव में कहना ग़लत नहीं होगा कि सभी प्रजातियों में बांज ही सबसे अधिक जानी भी जाती है और पाई भी जाती है। जानकारी मिलती है कि प्रायः 20 वर्ष पुराना होने पर बांज के पेड़ पर फल लगते हैं। पेड़ दो से तीन सौ वर्षों तक जीवित रहता है। इसकी ऊंचाई साधारणतया 100 से 150 फुट और घेरा 3 से 8 फुट तक होता है। कुछ बांज सफेद होते हैं, कुछ लाल या काले। कुछ बांजों से कॉर्क भी प्राप्त होता है। सफेद और लाल दोनों बांज अमरीका में उपजते हैं। भारत के हिमालय में केवल लाल या कृष्ण बांज उपजता है। बांज का काष्ठ 900 वर्षों तक अच्छी स्थिति में पाया गया है। काष्ठ सुंदर होता है और उससे बने फर्नीचर उत्कृष्ट कोटि के होते हैं।
एक समय जहाजों के बनाने में बांज का काष्ठ ही प्रयुक्त होता था। अब तो उसके स्थान पर इस्पात प्रयुक्त होने लगा है। आज मानव कुप्रभावों के कारण बांज के पेड़ शिकार हुए हैं और इसको बीजों को अनेक जंगली पशु खाते हैं और नष्ट करते हैं। विभिन्न कीटों, फंफूद व रोगों के कारण इस वृक्ष पर संकट बना हुआ है। फलियांट, फनियांट, हरिन्ज, रियाज, बांज, सांज बांज, तिलंज, मोरू, तिलोंज, खरसू या खरू बांज की ही विभिन्न प्रजातियां हैं, जो उत्तराखंड में मिलती हैं। पशुओं के भोजन से लेकर, कृषि यंत्रों के निर्माण, मकान निर्माण, ईंधन में बांज का प्रयोग किया जाता है। इस की हरी पत्तियों को पशुओं के चारे के रूप में तथा पत्तियों के गलने पर खाद के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इसकी इमारती लकड़ी बहुत काम की मानी जाती है।
आज भी उत्तराखंड के लोगों का प्रमुख धंधा कृषि और पशुचारण ही है। उत्तराखंड में दुधारू पशुओं भेड़, बकरियों, गायों की कोई कमी नहीं है और पशु चारे की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है जो कि वनों से ही पूरी की जाती है। भोजन पकाने के लिए भी ईंधन का विकल्प लकड़ी ही ज्यादा है। इसलिए शायद बांज के वनों का लगातार ह्वास हो रहा है। किसान भी खाद बनाने के लिए बांज की हरी व सूखी पत्तियों का अधिकाधिक उपयोग करते हैं तथा कृषि में काम आने वाले औजारों इत्यादि के लिए व ऐसे ही विविध उपयोगों में भी बांज की लकड़ी अपने निहित गुणों के कारण प्राचीन समय से उपयोग में आती रही है। शायद यही कारण है कि बांज पर खतरा मंडराने लगा है।
अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर इन बांज के पेड़ों को हम कैसे बचाएं ? तो इसका उत्तर यह है कि हम बांज के पेड़ों को काटे नहीं। केवल सड़ गल चुके पेड़ों व सूखे पेड़ों को ही मनुष्य द्वारा काम में लिया जाना चाहिए। अविकसित पेड़ों के विकास पर पर्याप्त ध्यान रखा जाना चाहिए। पेड़ों की वैज्ञानिक पद्धति से छंगाई कटाई की जानी चाहिए। ईंधन के विकल्प खोजें जाने चाहिए, यथा मिट्टी का तेल, गैस आदि का उपयोग किया जा सकता है। लकड़ी से बने कृषि यंत्रों के स्थान पर लोहे के कृषि यंत्रों को प्रयोग किया जाना चाहिए। वनों को दावानल (वनों की आग) से बचाया जाना चाहिए।
बांज के बीजों का वैज्ञानिक विधियों से रख रखाव किया जाना चाहिए और क्यारियां बनानी चाहिए ताकि हम इसका संरक्षण कर सकें। आज बांज के पेड़ काटने से वन एवं संसाधन धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। इसका प्रभाव विभिन्न जीव जंतुओं यथा भालू, बाघ, घुरड़, कांकड़, सुअर, थार आदि पर पड़ा है। जीव जंतुओं ही नहीं विभिन्न पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर भी बांज के पेड़ कटने का प्रभाव पड़ा है। पर्यावरण विकास और संतुलन को बनाए रखने वाले बांज के पेड़ों का संरक्षण आज समय की आवश्यकता है। इसे बचाया जाना हम सभी की जिम्मेदारी है।
लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं और वह दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।




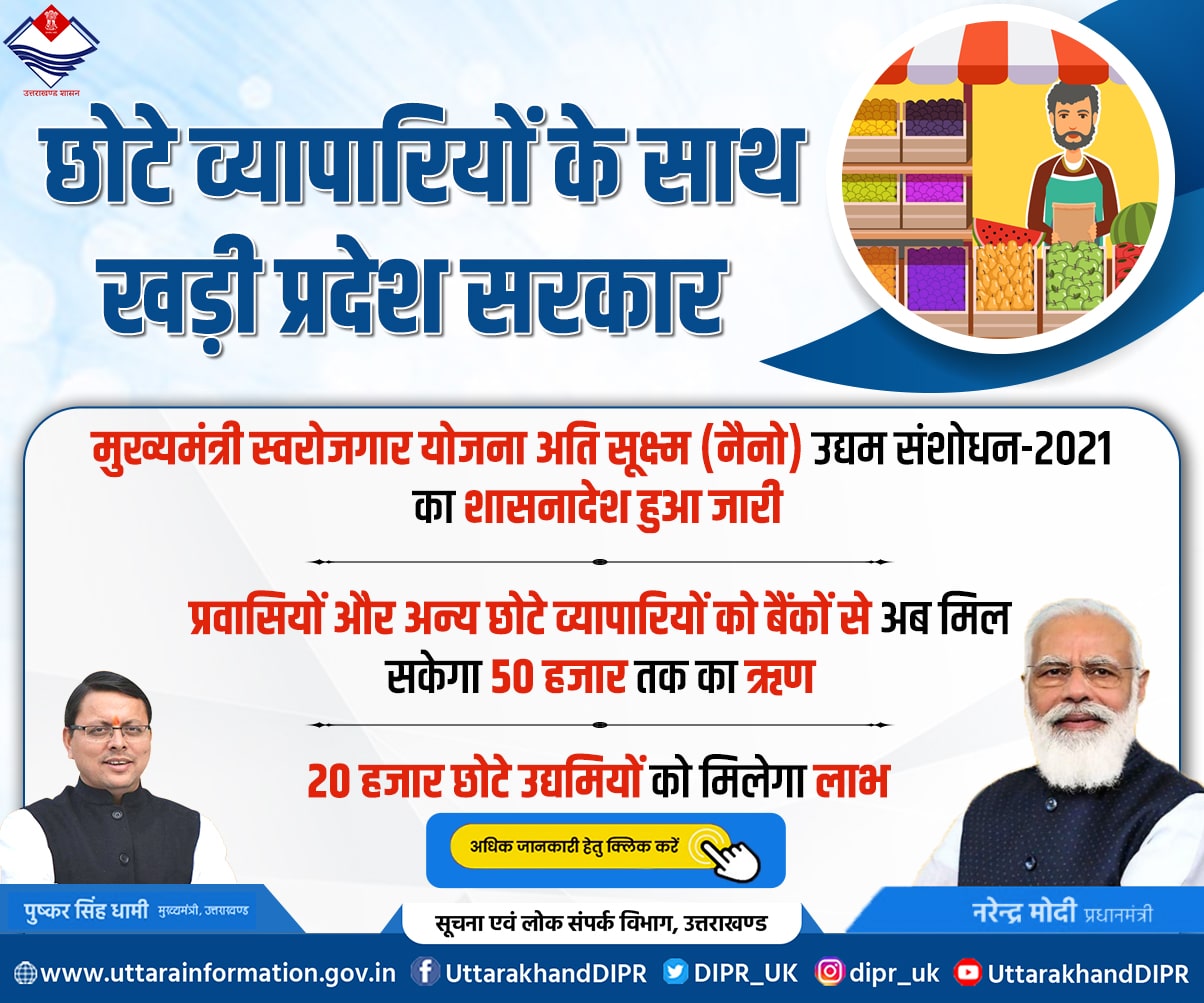
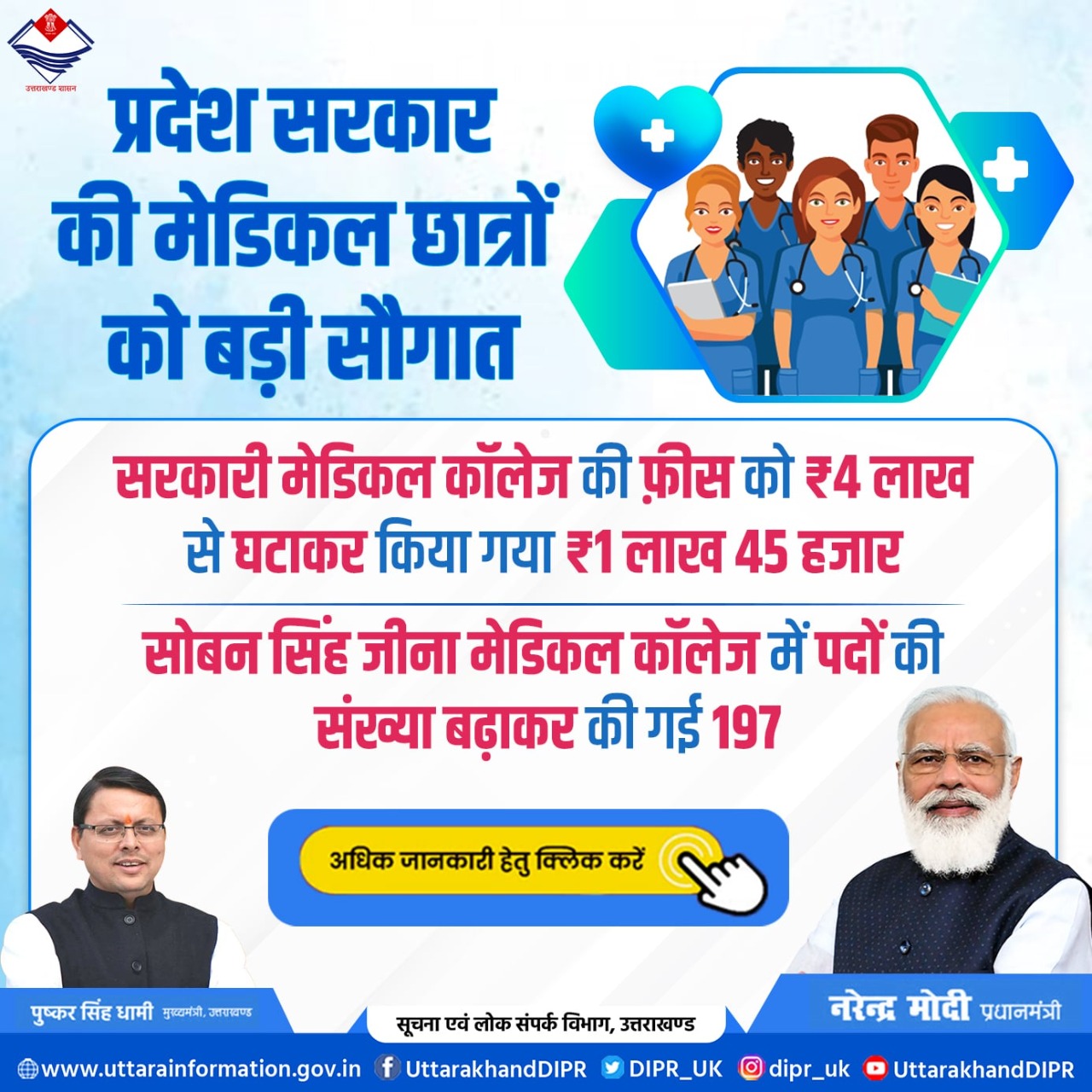



Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *