यह भू-कानून, जो प्रदेश के 11 पर्वतीय जिलों में गैर-नगरीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों द्वारा 250 वर्ग मीटर से अधिक कृषि भूमि खरीद पर रोक लगाता है, न केवल एक प्रशासनिक निर्णय है, बल्कि उत्तराखंड की जनता के दशकों लंबे आंदोलन का परिणाम भी है।
शीशपाल गुसाईं, देहरादून
हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक वैभव के लिए विश्व विख्यात है, लेकिन इस पवित्र भूमि की पहचान केवल इसकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा तक सीमित नहीं है, यह एक ऐसी धरती है, जहां की जनता ने अपनी अस्मिता, अधिकारों और संसाधनों की रक्षा के लिए बार-बार आंदोलनों का दामन थामा है। हाल ही में लागू हुआ उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025, जो राज्यपाल की मुहर के बाद 1 मई, 2025 से प्रभावी हो गया, एक बार फिर इस सतत संघर्ष की गवाही देता है।
यह भू-कानून, जो प्रदेश के 11 पर्वतीय जिलों में गैर-नगरीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों द्वारा 250 वर्ग मीटर से अधिक कृषि भूमि खरीद पर रोक लगाता है, न केवल एक प्रशासनिक निर्णय है, बल्कि उत्तराखंड की जनता के दशकों लंबे आंदोलन का परिणाम भी है। लेकिन,सवाल यह है कि क्या यह कानून वास्तव में पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण करता है, अथवा यह एक अधूरी विजय है, जो बार-बार आंदोलन की आवश्यकता को रेखांकित करती है?

भू कानून के बारे में कुछ तथ्य —
- 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने इस राज्य में शुरुआती दौर में भूमि खरीद पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं था।
- 2003 में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने बाहरी लोगों के लिए आवासीय उपयोग हेतु 500 वर्ग मीटर भूमि खरीद की सीमा तय की।
- 2008 में बी.सी. खंडूड़ी सरकार ने भूमि खरीद की सीमा को घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया।
- 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर उद्योगों के लिए जमीन खरीद की बाध्यताओं को हटा दिया।
- 2025 का भू-कानून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी के बाद विधानसभा के बजट सत्र में पारित करवाया।
- अब भू कानून में हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर को छोड़कर शेष 11 पर्वतीय जिलों में उत्तराखंड से बाहर के लोग कृषि और बागवानी भूमि नहीं खरीद सकेंगे।
- 250 वर्ग मीटर की सीमा तय की गई है, आवासीय उपयोग के लिए, जिसके लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य है।
भू-कानून का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और वर्तमान स्वरूप
उत्तराखंड के गठन के समय से ही भू-कानून एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने इस राज्य में शुरुआती दौर में भूमि खरीद पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं था। परिणामस्वरूप, उत्तराखंड से बाहर के लोगों ने, विशेषकर पर्यटन और रियल एस्टेट के आकर्षण के चलते, पहाड़ों की बेशकीमती जमीनों को सस्ते दामों में खरीदना शुरू किया। स्थानीय लोग, जो अपनी आजीविका के लिए इन जमीनों पर निर्भर थे, धीरे-धीरे भूमिहीन होने लगे।
2003 में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने बाहरी लोगों के लिए आवासीय उपयोग हेतु 500 वर्ग मीटर भूमि खरीद की सीमा तय की, जिसे 2008 में बी.सी. खंडूड़ी सरकार ने घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया। किंतु ये नियम नगरीय क्षेत्रों पर लागू नहीं थे, जिसके कारण देहरादून, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, जैसे शहरों के आसपास की जमीनें बड़े पैमाने पर बाहर के लोगों के हाथों में चली गईं। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने 2018 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन कर उद्योगों के लिए जमीन खरीद की बाध्यताओं को हटा दिया, जिससे बाहरी लोगों को अधिक जमीन खरीदने की छूट मिली। इस निर्णय ने व्यापक विरोध को जन्म दिया और मूल निवास 1950 की मांग को और बल मिला।

2025 का भू-कानून, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने पहले कैबिनेट में मंजूरी दी और फिर विधानसभा के बजट सत्र में पारित करवाया, एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर को छोड़कर शेष 11 पर्वतीय जिलों में उत्तराखंड से बाहर के लोग कृषि और बागवानी भूमि नहीं खरीद सकेंगे। आवासीय उपयोग के लिए भी 250 वर्ग मीटर की सीमा तय की गई है, जिसके लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य है।
यदि कोई व्यक्ति निर्धारित उद्देश्य से इतर भूमि का उपयोग करता है, तो वह सरकार में निहित हो जाएगी। यह कानून निश्चित रूप से स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग का परिणाम है, लेकिन इसकी सीमाएं भी स्पष्ट हैं। नगरीय क्षेत्रों को इस कानून के दायरे से बाहर रखने और हरिद्वार-ऊधमसिंह नगर जैसे मैदानी जिलों को छूट देने से यह आंशिक रूप से प्रभावी प्रतीत होता है।
- शहरी क्षेत्रों और मैदानी जिलों हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर को छूट देना भू कानून की सबसे बड़ी कमी।
- विडंबना है कि राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी जनता को अपनी जमीन, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ रहा।
- केवल 13.92 फीसदी मैदानी और 86 फीसदी पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण उत्तराखंड में कृषि भूमि पहले से ही सीमित है।
नरेंद्र सिंह नेगी और जन-आंदोलन की चिंगारी
उत्तराखंड की सांस्कृतिक आत्मा को अपनी गीतों में पिरोने वाले लोकप्रिय गढ़वाली गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने 2023-2024 में भू-कानून के समर्थन में अपने गीतों के माध्यम से जनता को सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। उनके गीत, जो पहाड़ की पीड़ा, संस्कृति और संघर्ष को व्यक्त करते हैं, उत्तराखंड के युवाओं और स्थानीय लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गए। देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, कोटद्वार, रामनगर जैसे शहरों में आंदोलनकारियों ने सशक्त भू-कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन किए, जो 1994 के उत्तराखंड राज्य आंदोलन की तर्ज पर थे। नेगी के गीतों ने न केवल जनमानस को जागृत किया, बल्कि यह भी रेखांकित किया कि पहाड़ की अस्मिता और संसाधनों की रक्षा के लिए एकजुटता आवश्यक है। उनके गीतों में छिपी पीड़ा यह थी कि बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध भूमि खरीद ने पहाड़ के मूल स्वरूप को खतरे में डाल दिया है।
पर्वतीय जनता के भाग्य में ‘आंदोलन ही आंदोलन’ क्यों?
उत्तराखंड की जनता का इतिहास आंदोलनों से भरा पड़ा है। 1970 के दशक में शुरू हुए चिपको आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण की वैश्विक मिसाल कायम की। 1994 का उत्तराखंड राज्य आंदोलन, जिसने अलग राज्य की मांग को साकार किया। पर्वतीय जनता ने अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए हमेशा सड़कों का सहारा लिया। किंतु यह विडंबना है कि राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी जनता को अपनी जमीन, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इसका एक प्रमुख कारण है प्रशासनिक मशीनरी की उदासीनता और कुछ हद तक स्थानीय लोगों की निष्क्रियता।
जैसा कि लेख में उल्लेख किया गया है, कई लोगों का मानना है कि यदि स्थानीय प्रशासन बाहरी लोगों के साथ सांठ-गांठ न करता, तो इतने बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद-फरोख्त संभव न होती। पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि की कमी और वहां की भौगोलिक परिस्थितियां इसे और जटिल बनाती हैं। केवल 13.92 फीसदी मैदानी और 86 फीसदी पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण कृषि भूमि पहले से ही सीमित है। प्रदेश से बाहर से आए लोगों के होटल, रिसॉर्ट और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन खरीदने से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका भी खतरे में पड़ गई।

उत्तराखंड में प्रमुख आंदोलन
- 1970 के दशक में शुरू चिपको आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण की वैश्विक मिसाल कायम की
- 1994 का उत्तराखंड राज्य आंदोलन, जिसने अलग राज्य की मांग को साकार कराया
जैसा कि पर्यावरणविद् रवि चोपड़ा, वरिष्ठ पत्रकार व लेखक जय सिंह रावत ने कहा, “राज्य में हर सरकार ने लोगों को धोखा ही दिया है।” नगरीय क्षेत्रों को इस कानून से बाहर रखना और हरिद्वार-ऊधम सिंह नगर जैसे जिलों को छूट देना इस कानून की सबसे बड़ी कमी है। देहरादून जैसे शहरों में नगर निगम की सीमा का विस्तार होने से आसपास के गांव अब नगरीय क्षेत्रों में शामिल हो चुके हैं, जिसके कारण वहां भूमि खरीद पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता। यह एक अधूरी पाबंदी है, जो भविष्य में और सशक्त कानून की मांग को जन्म दे सकती है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की जनता के भाग्य में ‘आंदोलन ही आंदोलन’ क्यों लिखा है? इसका उत्तर इस तथ्य में निहित है कि जब तक नीतियां और कानून जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप और पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होंगे, तब तक संघर्ष होगा।
हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सशक्त भू कानून है स्थायी समाधान
हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर एक सशक्त भू-कानून, जो न केवल पर्वतीय क्षेत्रों, बल्कि समस्त उत्तराखंड के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू हो, से ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते है-
- डिजिटल पोर्टल के माध्यम से बाहरी लोगों द्वारा खरीदी गई प्रत्येक इंच जमीन का रिकॉर्ड रखा जाए, जैसा कि सरकार ने प्रस्तावित किया है।
- गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।
- नरेंद्र सिंह नेगी जैसे सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से जनता को अपनी जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित किया जाए।
जब तक नगरीय क्षेत्रों और मैदानी जिलों को इसके दायरे में नहीं लाया जाता, तब तक यह आंशिक विजय ही रहेगी। उत्तराखंड की जनता का इतिहास बताता है कि वह अपनी अस्मिता और अधिकारों के लिए चुप नहीं बैठती। चिपको से लेकर राज्य आंदोलन और अब भू-कानून तक, यह धरती संघर्ष की धरती रही है। शायद यही इसकी नियति है—संघर्ष के माध्यम से अपनी पहचान को संरक्षित करना। किंतु यह भी सच है कि जब तक शासन-प्रशासन और जनता में पूर्ण समन्वय और जागरूकता नहीं होगी, तब तक यह सिलसिला थमेगा नहीं।


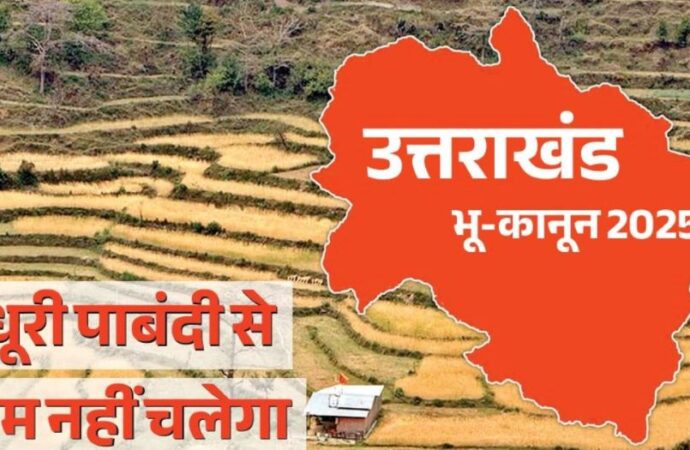

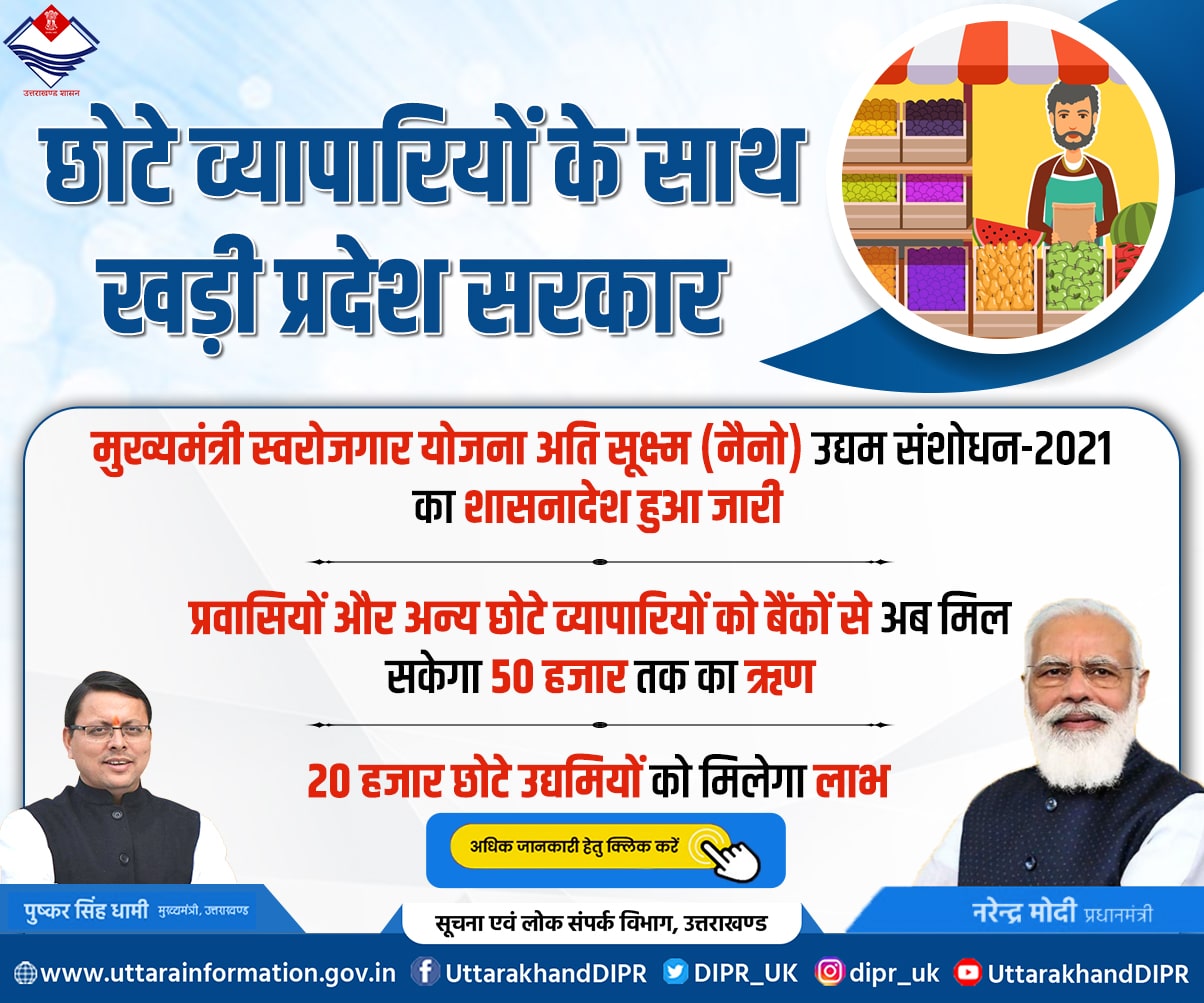
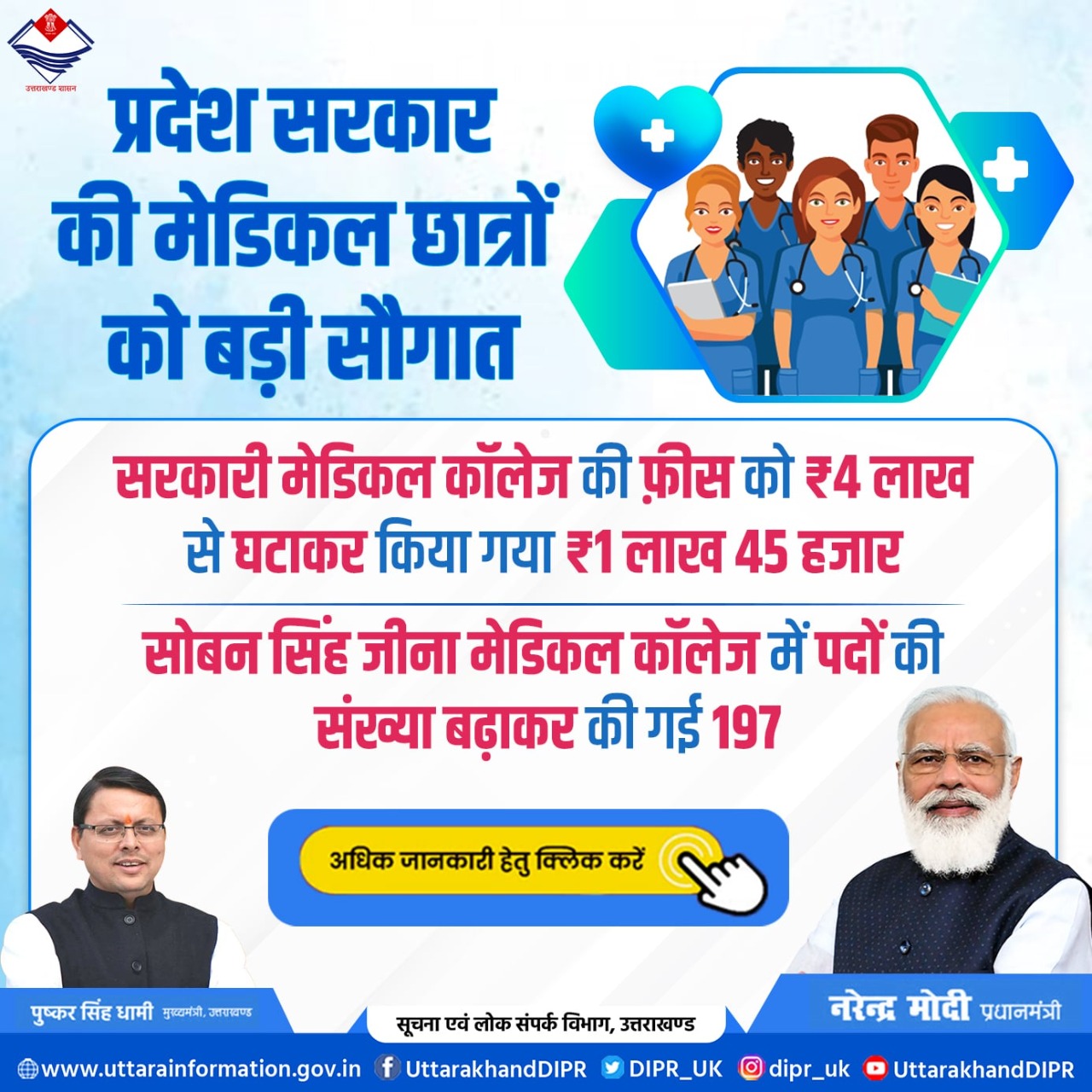



Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *